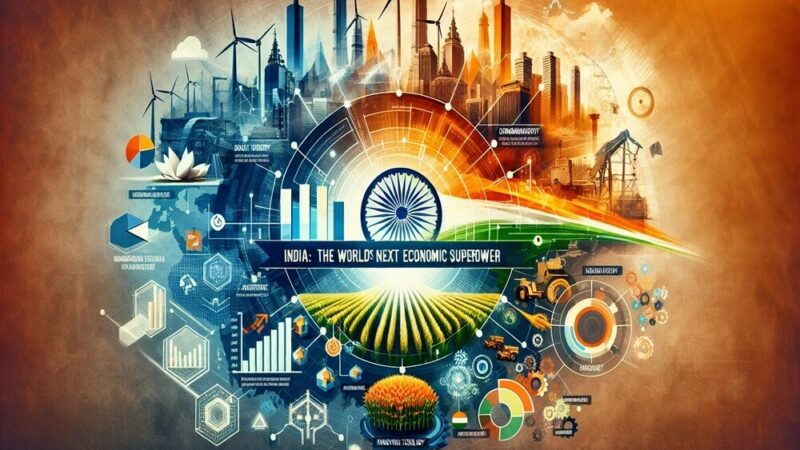विवाद: व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आमने सामने, संविधान की अनुच्छेद 368 पर मतभेद

अजय दीक्षित
तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा पेश और विधानसभा द्वारा पारित 10 बिलों को स्वीकृत करने में देरी को लेकर हफ्ते भर पहले सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई और सभी लंबित बिलों को खुद ही स्वीकृत कर दिया। इस याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्यपालों को लपेटे में लेकर कहा उन्हें किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य नहीं करना चाहिए।दूसरा उदाहरण वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी याचिका में सुनवाई कर दो अंतरिम आदेश दिए।इन दोनों घटनाओं से लुटियन्स में बबाल आ गया है। इसे व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में भीषण टकराव के रूप में देखा जा रहा है।
सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढ़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय संसद से पारित ओर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून में बदलाव नहीं कर सकती न ही रोक सकती ।अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि संविधान की अनुच्छेद 368 संसद को कोई भी कानून बनाने का अधिकार देती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोपरि है। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय की जू भी नहीं रेंग रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढ़ ने तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बरामद अधजले नोटों के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने वाला मामला भी उठाया।
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई 26 को रिटायर हो रहे हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की सुनवाई 05 मई को है ।
ऐसे में अगर कोई आदेश वक्फ संशोधन विधेयक याचिका में पारित हुआ तो केंद्रीय सरकार की किरकिरी होना तय है।
केशवानंद भारती विरुद्ध केरल सरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों वाली संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से आदेश जारी किया था कि संसद कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीन अंग हैं। व्यवस्थापिका के मुखिया राष्ट्रपति हैं ,जबकि न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख हैं। तीनों संस्थानों के अलग अलग कार्य हैं जिनमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति ज़बाबदेह है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। आजादी के बाद 26/01/1950 को संविधान बना और भारत गणराज्य बना। लेकिन जब तब व्यवस्था और ज्यूडिशियल की अप्रत्यक्ष लड़ाई विभिन्न मुद्दों पर देखने को मिलती है।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एक राष्ट्रीय लॉ कमीशन बनाना चाहती है और बना भी देते हैं मगर अंत में ज्यूडिशियल इस लॉ कमीशन को स्वत: ही संज्ञान में ले कर रद्द कर देती है। और दलील यह दी जाती है कि इससे संविधान की मूल ढांचे को क्षति होगी । न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। इसलिए कॉलेजियम ही न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए सही तरीका है।हालांकि जजों की नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकार, केंदीय सरकार से परामर्श लिया जाता है। सॉलिसिटर जनरल,राज्यों में अटॉर्नी जनरल की राय ली जाती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)